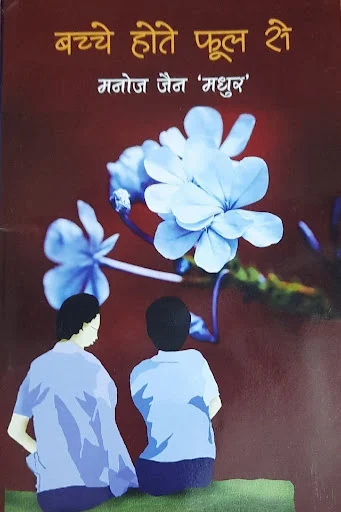" नीलकंठी प्रार्थनाएं " गीत-नवगीत संग्रह
रचनाकार : रघुवीर शर्मा
प्रकाशक : शिवना पेपरबैक्स
-वृहत समीक्षा-
समीक्षक : डॉ आलोक गुप्ता
मैंने श्री रघुवीर शर्मा को इससे पहले नवगीत कुटुंब के पटल पर ही पढ़ा था। जब उनकी पुस्तक को पूरा पढ़ लिया तो पाया कि यह ऐसा नवगीत-संग्रह है जो निरंतर प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा। "नीलकंठी प्रार्थनाएं" की समीक्षा करते हुए, मैंने एक पाठक के स्तर पर न केवल साहित्यिक कौशल में वृद्धि की बल्कि जीवन और मानवता के विभिन्न पहलुओं को भी गहराई से समझा।
इस पुस्तक की समीक्षा करते हुए, मेरा उद्देश्य रचनाकार की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का नहीं है। बल्कि, मेरा प्रयास है कि मैं उनकी इस पुस्तक की *सभी 67 रचनाओं* की ईमानदार और निष्पक्ष समीक्षा प्रस्तुत कर सकूं। मेरी समीक्षा का लक्ष्य है कि पाठक को पुस्तक की वास्तविकता से अवगत कराया जाए, जिससे वे इस पुस्तक को सही परिप्रेक्ष्य में देख सकें
1.*"नीलकंठी प्रार्थनाएं"* इस गीत-नवगीत संग्रह का सबसे पहला नवगीत है। यह समाज के उन पहलुओं को उजागर करता है जहां आम आदमी की प्रार्थनाएँ और आशाएँ अनसुनी रह जाती हैं। कवि के सपने और योजनाएँ कठोर और जड़ नियमों के कारण पूरे नहीं हो पा रहे हैं।
“नियम की अँधी गुफा में कैद है सब योजनाएँ
कागजों में स्वप्न अपने और कुछ विश्वास लिखकर
सौंप आए थे हमारे दर्द फिर कुछ खास लिखकर”
कवि ने सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना की है, जहां केवल दिखावा किया जाता है और वास्तविक समस्याओं को हाशिये पर रखा जाता है।
2.*“शुभचिंतक का बाना”* नवगीत में कवि ने समाज के उन लोगों को उजागर किया है जो शुभचिंतक का बाना पहनकर भोले-भाले लोगों का शोषण करते हैं। यह गीत प्रतीकात्मक रूप से समाज के उन दुष्ट व्यक्तियों और व्यवस्थाओं की ओर संकेत करता है जो दूसरों को धोखा देकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं।
दाने ऊपर जाल बिछाकर
भूखे पेटों को भरमाकर
फिर मुट्ठी में कैद करेंगे
आसमान के ख्वाब दिखाकर
3.*“कैसे गाएँ गीत”* इस नवगीत में कवि ने समाज के शोर-शराबे, रिश्तों की निस्सारता और सच्चाई की कमी को उजागर किया है। यह गीत समाज की उन बुराइयों और परेशानियों को उजागर करता है जो सृजनात्मकता, सच्चाई और प्रेम के अभाव के कारण उत्पन्न हो रही हैं। यह गीत एक सशक्त सामाजिक टिप्पणी है, जिसमें कवि ने समाज की वर्तमान स्थिति पर गहरा चिंतन किया है।
“शर्तों पर अवलंबित रिश्ते किसे बनाएँ मीत
इस बढ़ते कोलाहल में हम कैसे गाएँ गीत”
4.*“गूंगी पीड़ा”* यह गीत समाज की उन गहरी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करता है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती हैं। कवि ने कटे वृक्ष और सूखी नदियों की पीड़ा को व्यक्त किया है, जो पर्यावरणीय समस्याओं का संकेत है।
“कटे वृक्ष की गूंगी पीड़ा तपते जलते पाँव कहेंगे सूखी नदियों की जल गाथा बरसों प्यासे गाँव कहेंगे”
झुलसती उम्मीदों और राजनीतिक प्रक्रियाओं की मजबूरी की बात कही गई है। वहीं विज्ञापनों की खुशहाली को सत्ता की ओर से प्रचारित बताया गया है। गीत में सामाजिक असमानता और मेहनत की कम कीमत की ओरभी संकेत किया गया है। संविधान की अच्छी बातों और उनकी वास्तविकता में पालन न होने की बात कही गई है। कवि ने आगे उम्मीद और बदलाव की संभावनाओं की ओर संकेत किया गया है। अंत में दिशाहीन नेतृत्व और जनता के भटकाव की बात कही है।
5.*“नई जीवन शैलियाँ”*: इस नवगीत में कवि ने समाज में हो रहे परिवर्तनों और नई जीवन शैलियों को उजागर किया है, जो सतही और छलपूर्ण हैं। यह गीत समाज की उन बुराइयों और समस्याओं को रेखांकित करता है, जो आज की नई जीवन शैलियों में उभरकर सामने आई हैं। कवि ने नई जीवन शैलियों के चलन में आने की बात कही है। धनवान लोगों के मसीहा बनने की बात कही है, जो पैसे के बल पर समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं। धूर्त और झूठे लोगों की ओर इशारा किया है, जो बिना किसी कठिनाई के प्रभावशाली बन जाते हैं। अंत में, कवि ने ढोंग और पाखंड की स्थिति को उजागर किया है, जहाँ लोग वैराग्य का मुखौटा ओढ़कर मज़े कर रहे हैं।
“धूप से जो दूर हैं वे पसीने के प्रवक्ता
शब्द जिनके छल भरे बन गए वे प्रखर वक्ता
अब चलन में आ गई हैं, नई जीवन शैलियाँ
आवरण वैराग्य का हो रही रंगरेलियाँ”
6.*“समय कठिन है”* इस नवगीत में कवि ने कठिन समय की पीड़ा और संघर्षों को मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। यह गीत जीवन की उन परिस्थितियों को उजागर करता है, जहाँ हर दिन और हर रात एक नई चुनौती और कठिनाई के साथ आता है।
“समय कठिन है रात सुलगती तपता दिन है”
कवि ने कठिन समय की बात की है, जहाँ रातें और दिन दोनों ही कष्टदायक हैं। अफवाहों की तरह गर्म हवाओं का जिक्र किया गया है, जो हर सीमा को लांघ रही हैं। धूप को सुई की तरह चुभता हुआ बताया गया है, जो कठिन परिस्थितियों का प्रतीक है। रोटी की चिंता और दहशतपूर्ण दोपहर का जिक्र किया गया है। संध्याओं को भी संन्यासिन बताया गया है, जो बताता है कि शाम का समय भी कठिनाइयों से भरा हुआ है। उमस लिपटी विचलित रातों का जिक्र है, जो बेचैन और कष्टदायक हैं। अंत में, कवि ने कठिन समय के बावजूद उम्मीद को सुहागिन की तरह बताया है, जो आशा और भविष्य की संभावनाओं को जीवित रखती है।
7.*“हमने भी गरल पिया है”* नवगीत में कवि ने सरल और प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग करके जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों को बहुत ही मार्मिक तरीके से व्यक्त किया है कवि ने विषपान करने वाले नीलकंठ के प्रतीक का उपयोग किया है, जो यह दर्शाता है कि केवल एक व्यक्ति ही नहीं, बल्कि हर कोई अपने हिस्से का विष झेलता है। अच्छे और बुरे दिनों के मंथन की बात की गई है, जिससे उम्मीदों और इच्छाओं की कठिनाइयों को दर्शाया गया है। समय की उलझन और सरलता की कोशिशों की बात की गई है, जो जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों को दर्शाता है। जीवन की अनिश्चितता और निरंतरता का जिक्र किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि हमें भविष्य का पता नहीं होता। राहों के काँटों को फूल में बदलने की बात की गई है, जिससे हमारी मेहनत और प्रयासों का परिणाम बताया गया है।
“तुम ही नहीं हो नीलकंठ
हमने भी गरल पिया है
उलझा रहा समय उतना ही
जितना इसको सरल किया है”
8.*“खनक उठी साँकल”* नवगीत एक प्रेरणादायक और सकारात्मक संदेश देता है कि कठिनाइयों के बीच भी हमें आशा और खुशी के छोटे-छोटे क्षणों को पहचानना और संजोना चाहिए।
“बर्फीली देहरी पर ठिठकी हो क्षण भर
थकी हुई साँसों को मिला एक अवसर”
इसमें धूप के आँगन में उतरने और बादल के सावन में बरसने की बात की गई है, जो खुशी और आशा के आगमन का प्रतीक है। ठंडी सीमा पर क्षणिक राहत और अवसर का जिक्र है। अनमनी धड़कन में सरगम की लहर आने की बात है, जो अचानक आई खुशी और उमंग का प्रतीक है। वनवासी मन का घर लौटने की बात है, जो शांति और सुकून का प्रतीक है। संकल्प और समर्थन में साँकल की खनक का जिक्र है, जो नए अवसरों और खुशियों के आगमन का प्रतीक है।
“धीरे से उतर आई धूप घर आँगन में
चुपके से बरसी हो बदरी ज्यों सावन में”
9.*“हँसते गाते लोग”* नवगीत में कवि ने समाज में बदलते मूल्यों और रिश्तों की स्थिति को बहुत ही मार्मिक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। यह गीत हमें उन सरल और खुशमिजाज लोगों की याद दिलाता है, जो अपने जीवन की सरलता और सकारात्मकता से दूसरों को भी खुश रखते थे।
“जिनकी बतरस से अंसुआई आँखें हँसती थी
बिना साज के अनुभव की स्वर लहरी बजती थी”
कवि ने कबीरा जैसे हँसते-गाते लोगों की याद दिलाई है, जो जीवन की सरलता और आनंद को जीते थे। उनकी बातचीत और अनुभवों की स्वर लहरी का जिक्र किया गया है, जिससे लोग खुश हो जाते थे। उनके नित नए प्रयोगों से खुशियाँ बाँटने की बात की गई है। वर्तमान स्थिति का वर्णन किया गया है, जहाँ चौराहे सूने और चौपाल चुप है, और घर की बैठक अकेलापन और उदासी से बेहाल है। संवेदनशील रिश्तों पर स्वार्थ के रोग का जिक्र किया गया है, जो समाज के बदलते मूल्यों और रिश्तों की स्थिति को उजागर करता है।
10.*“छोटी-छोटी खुशियाँ”* गीत हमें याद दिलाता है कि जीवन में छोटी-छोटी बातों और क्षणों का कितना महत्व है, और कैसे ये छोटे-छोटे पल हमारे जीवन को सुंदर और आनंदमय बना सकते हैं।
छोटे-छोटे सपनों और खुशियों की बात की गई है, जो हमारे दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण बातें हैं। सोन चिरैया और मीठी धूप का जिक्र है, जो छोटे-छोटे आनंदमय पलों को दर्शाता है। थकी शाम और इंद्रधनुषी छवियों की बात है, जो संघर्ष के बाद के सुकून को दर्शाता है। पतझर के मौसम के बदलने और गीतों की स्वर लहरी में मन की बातें करने का जिक्र है, जो संगीत और बातचीत के माध्यम से खुशी पाने का प्रतीक है। पैरों में रुनझुन की बात है, जो छोटे-छोटे आनंदमय क्षणों को दर्शाता है।
“खुश हो
सोन चिरैया कुछ पल
आंगन में ठहरे
मीठी-मीठी धूप
मुंडेरों से नीचे उतरे
थकी शाम घर दिख जाए कुछ इंद्रधनुषी छवियाँ”
11.*“लुप्त हुई जीवन रेखाएँ”* गीत मानव-निर्मित पर्यावरणीय असंतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग के गंभीर परिणामों को व्यक्त करता है। है। कवि ने ऊँचे बाँधों के निर्माण से लेकर पानी की कमी से उत्पन्न समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया है। नदी की हरियाली मुरझाना, पक्षियों का गाना बंद होना, तालाबों में मछलियों का मरना और खेतों की फसलों का बर्बाद होना जैसे चित्रण पाठक के मन को गहराई से छूते हैं। गीत में नदी की स्थिति को मानवीकरण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जिससे उसकी दयनीयता और असहायता स्पष्ट होती है। कवि ने प्राकृतिक आपदाओं और मानव निर्मित समस्याओं के कारण बस्तियों के जीवन पर पड़े प्रभाव को भी दर्शाया है। यह नवगीत जल संकट और पर्यावरणीय समस्याओं का संवेदनशील और प्रभावशाली वर्णन करता है।
“शापित है खेतों की फसलें
बादल रूठे
मौसम बदले
खोज रही है
बस्ती इसमें
लुप्त हुई जीवन रेखाएँ।”
12.*“कृष्ण पक्ष अपने हिस्से है”*: यह गीत सामाजिक विषमताओं और असमानताओं पर एक कड़ा प्रहार है। कवि ने बहुत ही स्पष्टता और गहराई से सत्ता और आम जनता के बीच की दूरी, मीडिया की पक्षपाती दृष्टि, और आम लोगों के दुखों को चित्रित किया है। 'कृष्ण पक्ष' और 'धवल चाँदनी' के प्रतीकों का प्रयोग कर कवि ने सत्ताधारी और आम जनता के बीच की असमानता को बहुत ही प्रभावी तरीके से व्यक्त किया है।
“हम दुक्खों के बियाबान में उनके हाथों शकुनी पासा
सुख सुविधाएँ दासी उनकी अपने हक में महज दिलासा”
13.*“पारदर्शी आईने”* में कवि ने समाज में व्याप्त भौतिकवादी सोच पर टिप्पणी की है। आजकल श्रृंगार और सुंदरता का ध्यान केवल देह तक सीमित हो गया है, मन की सुंदरता का कोई महत्व नहीं रह गया। साथ ही, सद्भाव पर भी संदेह किया जाता है।
कवि ने स्वार्थ, धर्म, सत्य, सौंदर्य, और मूल्यों के बदलते मायनों को प्रभावशाली तरीके से उकेरा है। 'स्वार्थ के परिधान', 'धर्म का आवरण', 'पारदर्शी आईने', और 'मूल्य सजकर बाजार बिकने' जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल कर कवि ने समाज की वर्तमान स्थिति का सजीव चित्रण किया है।
“धर्म का आशय नहीं अब आचरण है
सियासत का महज यह आवरण
झूठ सच में भी रहा अंतर नहीं
भग्न है सब पारदर्शी आईने”
“स्वार्थ के नित नए परिधान पहने
खो रहे हैं शब्द अपने मायने”
14.*“अनघोषित संग्राम”* गीत समाज में मौनता और निष्क्रियता के खिलाफ एक कड़ा संदेश देता है। कवि ने निष्क्रियता को छोड़कर सच बोलने, झूठ को उजागर करने और सच्चाई के लिए लड़ने का संदेश दिया है। गंगाराम नामक प्रतीकात्मक पात्र के माध्यम से समाज के उन सभी लोगों को संबोधित किया है जो मौन और निष्क्रिय हैं। 'पत्थर के शालिग्राम', 'बाजीगर मौसम', और 'अनघोषित संग्राम' जैसे प्रतीकों का प्रभावी उपयोग किया गया है जो समाज की वास्तविक स्थिति को उजागर करते हैं।
“कब तक मौन रहोगे इस बाजीगर मौसम में
ठोकर खाते रहे सदा खुशहाली के भ्रम में
बने रहोगे कब तक पत्थर के शालिग्राम”
“कुछ ना कुछ तो कहना होगा तुमको गंगाराम”
15.*“बचा रहना चाहिए”* में कवि ने उन सभी चीजों का उल्लेख किया है जो अभी भी लोक जीवन में बची हुई हैं और जिनका बचा रहना बहुत महत्वपूर्ण है। हरापन (प्रकृति का सौंदर्य), अमराईयों (आम के पेड़ों) में बने घोंसले, नीम की ठंडी हवाएँ, और कोयल की मधुर आवाज़ - ये सभी प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरें हैं जिन्हें हमें संजोना चाहिए। कोयल की आवाज़ सुनना और उसकी मधुरता का आनंद लेना, यह दर्शाता है कि हमें प्रकृति की सुंदरता और लोक संस्कृति को महत्व देना चाहिए।
“हैं कहीं कायम अभी तक लोक-स्वर, लोक-भाषाएँ
आधुनिकता के हवन में जल न पाई जो कलाएँ
टिमटिमाते इन दीयों को जगमगाना चाहिए।”
नवगीत की भाषा सरल, सजीव और प्रभावी है। कवि ने हरियाली, अमराईयों के घोंसले, नीम की ठंडी हवाएँ, कोयल के गीत, लोक-स्वर, लोक-भाषाएँ, और टिमटिमाते दीयों जैसे प्रतीकों का बहुत ही सजीव और अर्थपूर्ण उपयोग किया है। यह प्रतीक हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर की सजीवता और सुंदरता को दर्शाते हैं।
16.*“अर्थ खोजते रहे”* गीत समाज की भाषा, विचारधारा, और उसकी जटिलताओं पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है। हम शब्दों के पीछे छिपे अर्थों को खोजते रहते हैं, लेकिन असली मंतव्य (उद्देश्य) और बात को समझना कठिन हो जाता है।
“क्या है असली मंतव्य और जाने क्या कहा गया है
वही अबूझी मीठी भाषा बस संदर्भ नया-नया है”
हम यह सोचते रहते हैं कि इसमें जनहित जैसा कुछ है, लेकिन यह सोच अक्सर व्यर्थ साबित होती है। कवि ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ बताया है कि कैसे भाषा और संदर्भ की जटिलता हमारे लिए असली मंतव्य को समझना मुश्किल बना देती है । लोग अक्सर शब्दों के सतही अर्थ से परे जाकर गहरे अर्थ की खोज में रहते हैं। यह हमारी मानसिकता को दर्शाता है जो सतही बातों से संतुष्ट नहीं होती और हमेशा गहरे अर्थ को समझने का प्रयास करती है। यह समाज की विचारशीलता की कमी और अनुकरणीयता को उजागर करता है।
“ज्ञानपीठ से व्याख्यानों में शब्दों का ताना-बाना
सत्य, धर्म और नीति-न्याय को राग-द्वेष में उलझाना
इस आयोजन में शामिल हम
जय बोलते रहे।”
17.*“उलझे समीकरण”* में कवि ने जीवन की कठिनाइयों और उनकी तुलना जटिल समीकरणों से की है। उन्होंने बताया कि कैसे खुशियों को जोड़ने की कोशिश में उम्मीदें घटती जाती हैं, और विषम दिनों की बढ़ती संख्या के कारण जीवन की संध्याएँ (शांतिपूर्ण समय) कम हो जाती हैं। कवि ने गणितीय चिंतन का उल्लेख किया है, जिसमें गुणा-भाग के बावजूद परिणाम हमेशा शून्य रहता है। सच्चे कार्यों का महत्व हाशिए पर ही रहता है और उनका महत्व नगण्य होता है। संतुलन के चिन्ह और जीवन की अज्ञात पहेली की बात की है, जो हमेशा हमें चुनौती देती रहती है। चर और अचर प्रथाओं के बीच संतुलन बनाए रखना भी एक कठिन कार्य है।
“चिन्ह संतुलन का बराबर (=) देख हमें हँस देता है
यह अज्ञात पहेली जैसा खूब परीक्षा लेता है
चर और अचर प्रथाओं के कोष्टक बंद चरण”
18.*“समय नहीं बदला”* में कवि ने बताया है कि दिन-प्रतिदिन तारीखें बदलती रहती हैं, लेकिन लोगों की स्थिति और समय की कठिनाइयाँ नहीं बदलतीं। पेट की धधकती आग (भूख) वही रहती है और हाथ हमेशा खाली रहते हैं। डाली पर सपनों की बाली (फसल) मुरझाई रहती है और संभावित फसलों पर मौसम का हमला होता रहता है, जिससे उनकी उम्मीदें धूमिल हो जाती हैं।
यह गीत हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं और कैसे सरकारी वादों और छद्म व्यवस्थाओं से धोखा खा जाते हैं। गीत की भाषा सरल और प्रभावशाली है, जो सीधे दिल और दिमाग पर असर डालती है।
“आधार पत्र की संख्या भर परिचय है अपना
मतदाता सूची में केवल नाम लिखा रहना
प्रजातंत्र का पारस, चिकना पत्थर ही निकला ।।”
19.*“कोमल आशाएँ”* में कवि ने किसानों की कोमल आशाओं का वर्णन किया है, जो उनके पसीने के साथ बह जाती हैं। फसलों के साथ बोए गए सपने फलते-फूलते नहीं हैं। श्रम से पोषित खेतों को हरियल (उपजाऊ) मौसम नहीं मिलता। बाजार की मनमानी (अनुचित मूल्य निर्धारण) के कारण किसानों की चिंताएँ और भी गहरी हो जाती हैं।
“संग पसीने के बह जाती हैं, कोमल आशाएँ
फसलों के संग बोए सपने फूले- फले नहीं
श्रम-पोषित खेतों को, हरियल मौसम मिले नहीं
बाजारों की मनमानी से गहराती चिंताएँ”
“कोमल आशाएँ” गीत किसानों की संघर्षपूर्ण जीवन की स्थिति का प्रभावी चित्रण है। यह गीत किसानों की कोमल आशाओं और उनकी वास्तविकताओं को सामने लाता है।
20.*“बूढ़े पेड़ पुराने”* में कवि ने बूढ़े पेड़ों की स्थिति का वर्णन किया है, जो अपनी पुरानी यादों में खोए रहते हैं। पहले ये पेड़ हरे-भरे थे और फूलों और फलों से लदे रहते थे। ये पेड़ जड़ों से जुड़े होने के कारण पतझड़ के हमलों से सुरक्षित रहते थे। अब वे पेड़ रातों में जागते हैं और पुराने दिनों को याद करते हुए सिरहाने रखते हैं। यह नवगीत बताता है कि पुराने समय की खुशहाल यादें अब उनके लिए केवल एक सपना बन गई हैं।
“यादों में खोए रहते हैं बूढ़े पेड़ पुराने
हरे-भरे थे, खूब लदे थे फूलों और फलों से
रहे सुरक्षित जड़ से जुड़कर पतझड़ के हमलों से
जाग रहे हैं अब रातों में वे दिन रख सिरहाने”
“बूढ़े पेड़ पुराने” गीत पुराने पेड़ों की स्थिति और उनकी यादों का सजीव चित्रण है। यह गीत हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे समय और परिस्थिति ने पेड़ों को अकेला और खाली कर दिया है, और वे पुराने दिनों की सुंदरता को याद करते हैं।
21.*“आई नहीं हवाएँ”* नवगीत में दर्शाने का प्रयास किया गया है कि आधुनिकता ने हमारे पारंपरिक जीवन के निशान मिटा दिए हैं। गाँव की पगडंडियों पर चलने वाली सभ्यता, चौपालों पर होने वाली चर्चाएं और हमारे पारंपरिक उत्सव सबकुछ बदल गया है। अब तिथि-उत्सव की जगह, केवल तारीखें बची हैं, जो समय की गणना भर रह गई हैं।
“ना पगडंडी की छाप, रही ना चौपालों की सीख तिथि-उत्सव के ऊपर आकर बैठ गई तारीख:
हमारी लोक कलाएँ और संगीत, जैसे बाँसुरी और मांदल के स्वर, अब कहीं खो गए हैं। पहले कच्चे मकान और घास-फूस के छप्पर थे, लेकिन रिश्ते बहुत मजबूत थे।
लाभ-हानि की सुबह-दोपहर मतलब की संध्याएँ”
आजकल हर किसी का जीवन लाभ और हानि, स्वार्थ और मतलब पर केंद्रित हो गया है। सुबह से शाम तक लोग अपने स्वार्थ और फायदे के लिए जीते हैं, जिससे मानवीय और भावनात्मक संबंधों की अहमियत कम हो गई है।
22.*“खुरदरा जीवन”* गीत जीवन की सच्चाई, संघर्ष और दर्द को सजीवता से व्यक्त करता है। इसमें कवि ने अपने जीए और सहे हुए अनुभवों को गीत के माध्यम से कहा है। खुरदरे जीवन की वास्तविकता को और लोकधर्मी चेतना की उधड़ती सीवन को दर्शाया है। समय के साथ जुड़े सच को अपने कथ्य में बयां किया है। समय के साथ प्रतिरोध का भाव व्यक्त किया है और अपने अनुभवों को झूमकर गाया है। कवि ने अपने दर्द को व्यक्त किया है, जो उसकी आँखों से बहा है। गीत की भाषा सरल और प्रभावशाली है।
“जो जिया है, जो सहा है
गीत में हमनें कहा है”
“टूट कर बिखरे नहीं हैं झूमकर गाया
शब्द में प्रतिरोध करना वक्त से पाया”
23.*“आसान नहीं है”* गीत जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों का चित्रण है। जीवन की राहें आसान नहीं हैं, खासकर सुख से जीने की। हमारी यात्राएँ सूरज के साथ ही शुरू होती हैं और दिनभर की मेहनत और संघर्ष के बाद हम रात में टूटे हुए सपनों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। कवि ने खुशियों के आँगन में भी काँटों (नागफनी) की उपस्थिति और आश्वासनों की चौसर पर उम्मीदों के सौदों की बात की है। सभी कठिनाइयों के बावजूद हम खुश हैं, संघर्षों में बड़े हुए हैं और समय को बदलने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं।
“सूरज के ही संग शुरू होती है यात्राएँ
परावलंबी सुबह
दोपहर नीरस संध्याएं
रातें होती हैं उधड़े सब सपने सीने की”
24.*“प्रश्न सड़क पर बिखरें हैं”* गीत सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की कड़ी आलोचना करता है। इसमें कवि ने नेताओं और अधिकारियों की असंवेदनशीलता, स्वार्थपरता और आम जनता की समस्याओं को सजीवता से चित्रित किया है।
“उत्तर बैठे हैं महलों में
प्रश्न सड़क पर बिखरे हैं”
कवि ने उत्तर और प्रश्न के बीच की दूरी को दिखाया है, जो कि समाज में व्याप्त असमानता को दर्शाता है। सरकारी आयोजनों और आम जनता की समस्याओं के बीच का अंतर दिखाया है। नेताओं की स्वार्थपरता और असंवेदनशीलता को उजागर किया है। समाज में धर्म और जाति की बेड़ियों और सच के नाम पर फैलाए जा रहे भ्रम की चर्चा हुई है। सच्चाई बोलने वालों की आवाज़ को दबाने की कोशिशों को चित्रित किया है।
25.*“पानी में कैसे रहना है”* गीत एक गहरी जीवन दर्शन की व्याख्या करता है जिसमें छोटी मछली के माध्यम से जीवन के संघर्षों और चुनौतियों का प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है।
“छोटी मछली समझ रही है
पानी में कैसे रहना है”
यह गीत बताता है कि कैसे हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, और सतर्क रहना चाहिए ताकि हम सुरक्षित और खुश रह सकें।
“मछुआरों के जाल परखती
काँटे से भी बचकर रहती
मगरमच्छ की नजरों में,
पर उसकी खुशियाँ रही खटकती”
26.*“मीठी नदिया हो जाती है”* गीत एक नारी के जीवन के विभिन्न पहलुओं का सुंदर और संवेदनशील चित्रण करता है। यह गीत नारी की संघर्षशीलता, त्याग, और सहनशीलता को दर्शाता है।
“मन का मौन सुने समझे हम
आँखों की अनबूझी भाषा
तपकर गल कर जिसने अपना
सुंदर घर संसार तराशा”
गीत में नारी के दुखों और संघर्षों के बावजूद उसके हँसते हुए चेहरे को दिखाया गया है। बेटी के बचपन से लेकर उसके शादी के बाद के जीवन तक की यात्रा का वर्णन है। उसके त्याग और नए रिश्तों में बँधने की बात की गई है और उसे पराया धन माने जाने की पीड़ा व्यक्त की गई है। उसकी सीमाओं और मर्यादा में बँधने का जिक्र है। उसकी अनकही भावनाओं और संघर्ष को समझने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। उसके सम्मान और सुरक्षा की महत्व को रेखांकित किया गया है। इस प्रकार, यह गीत नारी के जीवन के विभिन्न पहलुओं को संवेदनशीलता और समझदारी के साथ प्रस्तुत करता है। यह समाज को नारी की भावनाओं, त्याग, और संघर्ष को समझने और उसे सम्मान देने का संदेश देता है।
27.*“यह गेह तुम्हारा है”* गीत गौरैया (चिड़िया) के माध्यम से प्रकृति और मानव के बीच के संबंध को संवेदनशीलता से दर्शाता है। गीत में गौरैया को घर का हिस्सा माना गया है। उसकी चहचहाहट से आने वाले अपनापन और मिठास को सराहा गया है।
“चीं-चीं-चीं कर शब्दों में मीठापन ले आना
कोलाहल में भूल गए हम अपनापन गाना”
उसके आंगन में होने को विशेष बताया गया है। हरियाली की कमी के बावजूद उससे न दूर जाने का आग्रह किया गया है। उसकी उपस्थिति को सूखेपन से लड़ने का उपाय बताया गया है।
यह गीत सरलता और गहनता से प्रकृति के महत्व और मानव के साथ उसके संबंध को प्रस्तुत करता है।
28.*“पौधा खुशियों का”* नवगीत में माता-पिता के स्नेह और मार्गदर्शन की याद दिलाई गई है। जीवन की व्यस्तताओं के कारण उस स्नेह और सुख का आनंद न ले पाने की चर्चा की गई है और सपनों की खोज में घर छोड़ने और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की बात की गई है। सफर में दूर निकल जाने और वापस न लौटने का वर्णन हुआ है। जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करने का जिक्र किया गया है। अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की असमर्थता को दर्शाया गया है।
“नट जैसे रस्सी पर अब दम साधे चलते हैं
कठिन समय के समीकरण भी खुद हल करते हैं”
यह गीत हमें यह संदेश देता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां और संघर्ष क्यों न हों, हमें अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए और समय के समीकरणों को हल करने का प्रयास करना चाहिए।
29.*“सच अभय कहना है”* गीत में समय के साथ चलने और सत्य को निर्भय होकर कहने की प्रतिबद्धता को व्यक्त किया गया है। आधे-अधूरे उपायों से सच्चाई का सामना न करने की बात कही गई है। स्वयं दीप बनकर जलने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। समाज की अव्यवस्था और असत्य के फैलाव का वर्णन किया गया है। इस विकल दौर में सुरीला गीत रचने की इच्छा व्यक्त की गई है, जो समाज को सच्चाई और प्रेरणा का संदेश दे।
“भंग लय है, बेसुरा-सा स्वर उभरता है
पार्श्व में फिर छद्म देशी राग बजता है
विकल इस दौर में कोई सुरीला गीत रचना है”
यह गीत संदेश देता है कि सत्य और सच्चाई को निर्भय होकर कहना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो। हमें खुद में प्रकाश और साहस पैदा करना होगा, ताकि हम सच्चाई की राह दिखा सकें और समाज को एक नई दिशा दे सकें।
30.*“दीपक मिट्टी के”* गीत में कवि ने समाज की वर्तमान स्थिति और लोगों की उम्मीदों की टूटन को बखूबी व्यक्त किया है। इस गीत में रामराज्य की प्रतीक्षा में मिट्टी के दीपकों का वर्णन है, जो साधारण लोगों की आशाओं का प्रतीक हैं। दिखावे और छद्म रोशनी की आलोचना की गई है, जिससे सच्चाई और धार्मिकता दम तोड़ रही है।
“चकाचौंध है, छद्म रोशनी घर आंगन में पसरी
पूजा घर की ज्योति मद्धिम सांस ले रही गहरी”
झोपड़पट्टी के लोगों की निराशा को व्यक्त किया गया है। आदर्श और सपनों की खोई हुई स्थिति और राजनीति की चालबाजियों का वर्णन है। लोगों के सपनों की टूटन और उनकी निराशा को दर्शाया गया है।
यह गीत समाज की सच्चाई, दिखावे, राजनीति की चालबाजियों और साधारण लोगों की निराशा को उजागर करता है। कवि ने बहुत ही सुंदरता से यह दिखाया है कि कैसे सच्चाई और उम्मीदें छद्म रोशनी और झूठे वादों के बीच दम तोड़ रही हैं।
31.*“रामचरितमानस पढ़ते हैं”* गीत में कवि ने तुलसीदास जी की रामचरितमानस के महत्व, समाजिक और राजनीतिक स्थिति की समीक्षा, धार्मिक आदर्शों के महत्त्व और असली बदलाव की आवश्यकता पर गंभीरता से बात की है। गीत में प्रत्येक छंद का उपयोग उस विशेष समय की स्थिति और समस्याओं को समझाने में किया गया है, जो सामाजिक और धार्मिक संकटों का सच्चा चित्रण करता है।
“केवल पुतलों के जलने से असली रावण कब मरते हैं।“
32.*“दुम हिलाओ”* गीत में व्यापक समाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आम लोगों को बस चुपचाप समर्थन करने और कोई सवाल न उठाने के लिए कहा जा रहा है। उनसे कहा जाता है कि वे अपनी भूख और अन्य समस्याओं को नजरअंदाज करें क्योंकि नेताओं और अधिकारियों के पास अपनी छवि सुधारने और अपनी कुर्सी बचाने का काम अधिक महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर, यह कविता उस विडंबना और ढोंग की ओर इशारा करती है जिसमें जनता की वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है और उन्हें केवल समर्थन करने और सवाल न उठाने के लिए कहा जाता है।
“क्यों तुम्हारे पास फिर इतनी शिकायत है महज कर्त्तव्य की जब तुमको हिदायत है”
33.*“पुरानी डायरी”* गीत अपनी पुरानी डायरी के माध्यम से व्यक्ति के अंतर्निहित भावनाओं को उजागर करता है और उसके अनुभवों को ताजगी से भरता है। गीत अपने अलंकरण से भरपूर है और व्यक्तिगत अनुभवों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है। प्रत्येक छंद व्यक्ति की भावनाओं और अनुभवों को समझाने में मदद करता है और उसकी भावनाओं को साहित्यिक रूप में उकेरता है।
“पृष्ठ से कुछ महक आती है, पसीने से भरी
34.*“पसीना आ रहा है”* यह गीत समाज में हो रहे बदलाव को, खुशियों और दुःख के विपरीत स्थितियों को दर्शाता है और उनके माध्यम से व्यक्ति की अंतर्निहित भावनाओं को बयान करता है। समाज में बदलाव का वर्णन है, जहां पुरानी खुशियाँ और स्थानिकता की कमी महसूस हो रही है।
“बिक रही बाजार, खुशियाँ सजी दुकानों में अब नहीं मिलती, पुरातन ठौर-ठिकानों में”
35.*“बटन पर आश्रित उजाले”* गीत में आधुनिक जीवनशैली और परिवर्तन के प्रति एक व्यक्ति की चिंताओं का विवेचन किया गया है। व्यक्ति के मन की स्थिति और उसके अंतर्निहित भावनाएं की बात की गई है, जो आधुनिकीकरण और परिवर्तन के कारण उसके मन को प्रभावित कर रहे हैं। समाज के आधुनिक उत्सवों की बात की गई है, जो व्यक्ति के जीवन में एक परिवर्तन लाते हैं। समाज में बदलाव के संदर्भ में बात की गई है, जो परंपराओं और अनुसरणीय सेतुओं को ढहा देता है।
“मन हुलसता ही नहीं, फिर कौन किस पर रंग डाले दीप माटी के कहाँ, अब बटन पर आश्रित उजाले”
36.*“आँधियों का शोर है”* गीत में प्राकृतिक तत्वों की बदलती हुई स्थिति और उनके संवाद का विवरण है, जो समाज और मानवता के साथ कवि के गहरे संवाद में हैं। नवगीत में जहाँ आँधियां एक ध्वनि की तरह हैं और हवाएं शांत हैं, वहीँ पेड़ अपनी अस्थिरता को दर्शाते हैं और धूल के चक्रवात में दिशाएँ ओझल हो जाती हैं। आकाश में गरजन और बादलों की दौड़ को दर्शाते हुए, प्राकृतिक आपदाओं की ओर भावनात्मक रूप से इशारा किया गया है और वनों में पंछियों की अप्राप्तता का वर्णन है।
“पेड़ है बेचैन सारे टहनियां टकरा रही हैं और हाहाकार में स्वर कोकिला घबरा रही है”
37.*“हमें पता है”* गीत में व्यक्ति की आत्म-समझ, स्वाधीनता, और साहस का वर्णन किया गया है। रचनाकार ने अपनी उलझन को समझने और हल करने की बात की है, जो स्वाधीनता और स्वायत्तता को दर्शाता है। व्यक्ति की निर्णायकता और स्वतंत्रता का वर्णन है, जो अपने मार्ग को अपनी मातृभूमि के अनुसार चुनता है।
अपनी मुश्किल अपने दुखड़े अपने तक रखते हैं अगर मुखर हो कह दें, तो वे सौदा ही करते हैं
38.*“जुगनू देख रहे हैं”* गीत में सूर्योदय, जुगनू, भोर के सितारे, और आसमान की तिर्यक रेखाएं जैसे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया गया है। गीत में सूर्योदय की आशा को जुगनू के दृष्टिकोण से व्याख्यानित किया है जहाँ जुगनू रात के अंधेरे में चमकते हैं, और उनके द्वारा सूर्योदय की आस दिखाई दी है। भोर के सितारों के बारे में बात की है, जो बादलों की साजिश को भ्रमित करते हैं। आसमान की तिर्यक रेखाओं का जिक्र है, जो अनियमितता और अस्थिरता का प्रतीक हैं।
“देख रहे हैं खूब प्रचारित
बिना अर्थ के उजियारों को
पीले बादल की साजिश को
भरमाते भोर सितारों को”
39.*“लाठी हाथ लिए”* एक नवगीत है जो समाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है। भेड़ों की चाल के माध्यम से व्यक्ति के नियंत्रण के बारे में बात की गई है, जिसमें उन्हें मालिक की मर्जी के अनुसार जीना पड़ता है। , जो उनकी लाचारी को दर्शाता है। व्यक्ति की अवस्था के बारे में बात की गई है, जब उन्हें अपने तन का ऊन देना पड़ता है, जो उनकी मजबूती का प्रतीक होता है।
“भेड़ चाल लाचारी उसकी पेट सभी को भरना है
गुजर नहीं होगी, बिन अपने तन का ऊन दिए”
40.*“बेसुध हैं हम लोग”* में समाज की स्थिति को व्यक्ति और समूह के स्तर पर व्याख्यात किया है, जिसमें सत्ता, धर्म, जाति और धन-संपत्ति के प्रभाव को दिखाया गया है। गीत में व्यक्ति या समूह की स्थिति का वर्णन है, जिसे सियासत के द्वारा बेहोश बना दिया गया है। समाज को धर्म, जाति और समृद्धि के नशे में डूबा दिया गया है। समाज में व्यक्ति की अवस्था ऐसी हो गई है कि मानो वह षड़यंत्रों (चालाकी) के बवंडर से बेहोश हो चुका है।
“भांग सियासत की पीकर बेसुध हैं हम लोग
सत्ता भर हथियाने के आयुध हैं हम लोग”
41.*“उत्तरों की आस में”* गीत में व्यक्ति की प्रार्थनाएँ फाइलों में बंद हो रही हैं । वह प्रश्नों के उत्तर की आशा में हैं, लेकिन प्रश्न अभी तक खारिज हैं। सामाजिक या राजनीतिक स्थिति में कुछ ऐसा हो रहा है जो लोगों के विश्वास को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है।
“प्रश्न खारिज, और हम हैं उत्तरों की आस में
मूल प्रश्नों पर कहाँ होती है चर्चाएँ
शोर करती और फिर स्थगित होती सभाएँ
है अनुत्तरित मुद्दे हर किसी के पास में”
42.*“पथ पर नहीं रुके हैं हम”* एक गीत है जो यह बताता है कि आम जनता ने नेताओं और उनके वादों की असलियत को समझ लिया है। उन्होंने अपने संघर्षों में हार नहीं मानी है और न ही कभी झुके हैं। यह कविता उन नेताओं की आलोचना करती है जो सत्ता में आकर अपने वादों को भूल जाते हैं और केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं।
“जान गए हैं विकास की गंगा किस तट थमी हुई है
खुशहाली भी कहाँ-कहाँ किस-किस ठौर रमी हुई है
मन पर बोझ लिए चलते हैं पथ पर नहीं रूके हैं हम ।।“
43.*“छलिया खेले खेल”* का सार यह है कि राजनीति में छल-कपट और चापलूसी का बोलबाला है। नेता मीठी-मीठी बातें करके जनता को धोखा देते हैं और सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। जनता भूखी-प्यासी रह जाती है और उनके नारे भी उनके पेट नहीं भरते। लोकतंत्र के चारों स्तम्भ (संविधान, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया) नेताओं के सामने नतमस्तक हैं और उनके कृत्यों पर अंकुश लगाने में विफल हैं। गाँवों और नगरों में भी चापलूसी का माहौल है और नेता गुस्से में रहते हैं।
“भूखे प्यासे झंडा लेकर
पेट भर रहे नारे खाकर
डाले कौन नकेल”
44.*“उपवन बहुत उदास है”* नवगीत का मुख्य भावार्थ यह है कि समाज में अव्यवस्था और पीड़ा फैली हुई है। समाज (उपवन) उदास और भयभीत है, नए और मासूम लोग (खिलती कलियाँ) डरे हुए हैं। माली (प्रशासन) अपने कर्तव्यों से बेखबर है, और हर व्यक्ति दर्द सह रहा है। समाज की शुद्धता नष्ट हो चुकी है, और बड़े-बड़े लोग भी लाचार हो गए हैं। नियम और कायदे भी व्यापार का हिस्सा बन गए हैं, और सब लोग उस व्यापार के दास हो गए हैं। यह कविता समाज की स्थिति पर गहरा कटाक्ष करती है और उसकी वास्तविकता को उजागर करती है।
“उपवन बहुत उदास है
आतंकित है खिलती कलियाँ / सिहराती है चहल कदमियाँ
काँटे भी आसपास हैं”
45.गीत *“वसंत आया है”* में वसंत ऋतु का आगमन तो हुआ है, लेकिन यह केवल बाहरी दिखावे तक सीमित है। अखबारों में रंग-बिरंगे चित्र हैं, लेकिन मन में खुशी नहीं है। समाज में गमले के पौधे (लोग) उदास और निढाल हैं, और उपवन (समाज) मुरझाया हुआ है। वन टेसू का मुस्कराना इस बात का प्रतीक है कि कहीं न कहीं थोड़ी बहुत खुशी है, लेकिन संपूर्ण समाज में वह खुशी महसूस नहीं हो रही है। गीत समाज की आंतरिक उदासी और बाहरी दिखावे के बीच के विरोधाभास को उजागर करता है।
“यह कैसा वसंत आया है
अखबारों के पृष्ठ रंगे हैं अमराई के चित्र टंगे हैं
मन मगर कहाँ हुलसाया है”
46.*“बरसो बादल”* नवगीत में समाज और उसकी व्यथा को उपवन (बगीचे) के रूपक के माध्यम से व्यक्त किया गया है। समाज में अव्यवस्था और पीड़ा फैली हुई है। समाज (उपवन) उदास और भयभीत है, नए और मासूम लोग (खिलती कलियाँ) डरे हुए हैं। माली (प्रशासन) अपने कर्तव्यों से बेखबर है, और हर व्यक्ति दर्द सह रहा है। समाज की शुद्धता नष्ट हो चुकी है, और बड़े-बड़े लोग भी लाचार हो गए हैं। नियम और कायदे भी व्यापार का हिस्सा बन गए हैं, और सब लोग उस व्यापार के दास हो गए हैं।
“नन्हीं कलियों के सपने पेड़ों के भी दुख अपने
भंग हुई है लय नदियों की ठिठक खड़े हुए हैं झरने
अब तक केवल शेष रहा है हलधर की आँखों का जल ।।“
47.*“बादल आए हैं”* इस नवगीत में कवि ने वर्षा के आगमन से उत्पन्न होने वाली खुशियों और उत्सव का सुंदर वर्णन किया है। प्रकृति का मानवीकरण करते हुए, उन्होंने बादलों को समुद्र का संदेशवाहक, बारिश की आवाज़ को शहनाई और बूंदों को शुभ संदेश वाहक के रूप में प्रस्तुत किया है। गीत में नदियों, खेतों, वन-क्षेत्र, घर-आँगन, और गली-गली का चित्रण कर पूरे वातावरण में उत्सव और खुशी का माहौल बनाया है।
“अँकुराई आशाएँ नदियों की आँखें भर आई
छत पर अविरल गूँज रही है बूंदों की शहनाई
घट भर दौड़ दौड़ कर दल के दल आए हैं”
48.*“क्यों कर बदल गए”* यह गीत गाँव के बदलते स्वरूप और उसकी पुरानी सादगी के खो जाने पर चिंता व्यक्त करता है। गीत की भाषा सरल और प्रभावशाली है, जो सीधे दिल को छू जाती है। नदियों, अमराइयों, खेतों और लोक पर्वों का उल्लेख करते हुए गीत गाँव की पुरानी जीवनशैली और उसकी सादगी को याद दिलाता है। इसके साथ ही, गीत में आधुनिकता के प्रभाव और गाँव के लोगों के बदलते मूल्यों पर भी ध्यान आकर्षित किया गया है। बाजार की चकाचौंध और टी.वी. की नकली मुस्कानों के पीछे भागते हुए गाँव ने अपनी पुरानी परंपराओं और सादगी को खो दिया है।
49.*“हे! नववर्ष”* : यह गीत नववर्ष के स्वागत और उससे जुड़ी उम्मीदों और प्रार्थनाओं को बेहद संवेदनशील और भावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करता है। गीत में नववर्ष से न्याय, समानता, और समृद्धि की प्रार्थना की गई है। यह उन लोगों के लिए भी खुशहाली की कामना करता है जो संघर्षरत हैं और जिनकी आँखों में नमी है। गीत आत्म-निरीक्षण का भी संदेश देता है, जिसमें बीते हुए वर्षों की भूलों और चूकों पर विचार किया गया है।
“गत वर्षों में भूले क्या? चूक कहाँ पर हुई
जगमग जीवनमूल्यों की चमक कहाँ खो गई
मानवता के हित में हो सार्थक कोई विमर्श।।“
50.*“अपना देश”* यह गीत भारत के प्रति गहरी प्रेम और सम्मान की भावना को व्यक्त करता है। गीत में देश की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर, और महान संतों और कवियों की विरासत का उल्लेख है। गीत में प्रेम, श्रद्धा, और सम्मान की भावना स्पष्ट रूप से झलकती है, जो हर भारतीय के दिल में बसे देशभक्ति के जज्बे को प्रकट करती है।
“मुझको प्यारा लगता, अपना देश है
अपनी माटी है, अपना परिवेश है
गंगा, यमुना, कावेरी
रेवा का निर्मल नीर है
विंध्याचल, सतपुड़ा मेखला हिमगिरि दृढ़ गंभीर है”
51.*“माँ- बाबूजी ही दिखते हैं”* यह गीत हमें हमारे माता-पिता के प्रति सम्मान और प्रेम की गहरी भावना से भर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे माता-पिता का योगदान हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और उनकी यादें हमें हमेशा प्रेरित करती हैं। यह गीत उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो अपने माता-पिता की यादों को संजोकर रखते हैं और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं।
“गए नहीं है माँ- बाबूजी हर पल घर में ही रहते हैं
माँ के स्वर में बहन-बेटियाँ उच्च नीच समझाती हैं
बाबूजी की सीखें मेरी हर उलझन सुलझाती हैं”
52.*“याद की खुशबू”* यह गीत हमें यादों की महक, प्रेम की सुंदरता और उसकी ताजगी को अनुभव कराता है। गीत के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि प्रेम की यादें हमेशा ताजगी और जीवन की खुशबू के साथ हमारे साथ रहती हैं। यह गीत न केवल प्रेमियों के लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है, जिसने कभी प्रेम किया है और उसकी यादों को संजोकर रखा है।
“लिपटकर फिर फूल से ज्यों
हुलसकर बतिया रही हो तितलियाँ
आरोह से अवरोह तक स्वांस स्वर में धुन उतरती है
मौन आधारों पर कोई मृदु गीत की पंक्ति उभरती है”
53.*“प्रिये तुम्हारी प्रीत”* यह गीत प्रेम, समर्पण, और धैर्य का उत्कृष्ट चित्रण करता है। प्रेयसी का प्रेम और उसका जीवन के प्रति समर्पण इस गीत में बखूबी व्यक्त किया गया है। यह गीत उनके संघर्षों, कठिनाइयों, और धैर्य को सजीव रूप में प्रस्तुत करता है।
“माथे पर श्रम-सीकर फिर भी अधरों पर मुस्कान कई अभावों को जी कर भी आँखों में सम्मान
ताने, सिकवों में भी मीठा बजता है संगीत”
गीत की भाषा सरल और भावपूर्ण है, जो दिल को छू लेने वाली है। हर छंद में प्रेयसी के समर्पण और उसकी निस्वार्थ प्रेम को व्यक्त किया गया है। गीत सावित्री-सत्यवान की पौराणिक कथा का संदर्भ देकर प्रेम और समर्पण की गहराई को और भी प्रभावी बनाता है। यह गीत न केवल प्रेयसी के प्रति प्रेम को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि सच्चा प्रेम किस प्रकार हर कठिनाई को पार कर सकता है। यह गीत उन सभी को प्रेरित करता है जो अपने जीवन में प्रेम और समर्पण की तलाश में हैं।
54.*“यह समय कितना कड़ा है”*
यह गीत कोरोना महामारी के दौरान उत्पन्न हुई कठिनाइयों, अनिश्चितताओं, और भय को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। गीत की पंक्तियाँ दर्शाती हैं कि यह समय कितना कठिन है और सभी को इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। यह महामारी ने समाज की व्यवस्थाओं की कमजोरियों को उजागर किया है और बताया है कि कैसे एक
“छोटा सा वायरस पूरी दुनिया के लिए बड़ा संकट बन गया है।
यह समय कितना कड़ा है। सामना जिससे पड़ा है।
इस भयावह दौर की हैं अनकही सब की कहानी।
है धरातल पर अपाहिज व्यवस्थाएँ आसमानी।
एक छोटा वायरस भी हो गया कितना बड़ा है।“
55.*“भूखा पेट गरीब का (कोरोना प्रसंग)”* यह गीत कोरोना महामारी के दौरान गरीब मजदूरों की स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। गीत में उनकी उम्मीदों और वास्तविकता के बीच के अंतर को भी दर्शाया गया है। यह बताया गया है कि कैसे वे मेहनत और हौसले के साथ अपने सपनों को साकार करने की उम्मीद में थे, लेकिन महामारी के तूफान ने उनकी सारी उम्मीदों को तोड़ दिया। उनके सामाजिक अनुभवों का वर्णन करते हुए गीत ने यह भी बताया कि उन्हें केवल डाँट-डपट और झिड़कियाँ मिलीं, लेकिन कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ।
“लौट कर घर आ रहे हैं छोड़कर सब नसीब का
हौसला तो था किनारे पहुँच जाएंगे
था न पता माझधार में तूफान आएंगे
डाँट-डपट झिड़की मिली
मिला न कोई करीब का।“
56.*“प्रश्न समय के”* यह गीत कोरोना महामारी के दौरान उत्पन्न अनिश्चितताओं, षडयंत्रों, और लोगों के टूटते विश्वास को दर्शाता है। इसमें कहा गया है कि कैसे महामारी ने समाज की तहजीब को खंड-खंड कर दिया है और लोग भय और संशय के दिनों में जी रहे हैं। गीत का केंद्रीय संदेश यह है कि महामारी ने न केवल भौतिक बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी गहरा प्रभाव डाला है।
“जहरीले अणुओं की लुका-छुपी जारी है
मेहनत पर आदमखोर आंकड़े भारी है
छंद बिखर गए जीवन लय के”
57.*“डर बाहर भीतर”* यह गीत कोरोना महामारी के दौरान उत्पन्न भय और चिंताओं को दर्शाता है। गीत की पंक्तियाँ सजीव चित्रण करती हैं कि कैसे सड़के और गलियाँ सूनी हो गई हैं और लोग अपने-अपने घरों में कैद हो गए हैं। गीत का अंत सकारात्मक और आशावादी है, जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि यह कठिन समय भी हमारे दृढ़ संकल्प और सही उपायों से हार जाएगा।
“धीरे धीरे फैल गया है डर बाहर भीतर
सड़के सूनी गलियाँ सूनी सूने आंगन द्वार
कैद हो गए अपने घर में भय शापित परिवार
शंकाओं का बीजारोपण है मन के अंदर”
58.*“ऊँचे आसन से”*: यह गीत अयोध्या प्रकरण पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद उत्पन्न हुए सकारात्मक परिवर्तन और भावनाओं को दर्शाता है। कवि ने बड़े ही संवेदनशील और प्रभावशाली तरीके से इस फैसले के बाद समाज में उत्पन्न हुए प्रेम, एकता और भाईचारे की भावना को व्यक्त किया है। यह गीत हमें यह संदेश देता है कि कैसे न्याय और समझदारी से लिए गए फैसले समाज में प्रेम और एकता का वातावरण बना सकते हैं। यह एक प्रेरणादायक गीत है जो हमें सिखाता है कि नफरत को कैसे प्रेम और समझदारी से मिटाया जा सकता है।
“कुछ किरणें आई हैं सूरज के ऊँचे आसन से
मतभेदों की जमी बर्फ फिर धीरे-धीरे पिघली
साफ हुई मन की मैली काई, सब अगली पिछली
धुली नफरतें धरती की अनुराग भरे सावन से”
59.*“लोकतंत्र का उत्सव”*
यह गीत हमें आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हम वाकई अपने लोकतंत्र और उसके मूल्य को समझते हैं, या केवल प्रतीकात्मकता तक ही सीमित हैं। कुल मिलाकर, यह गीत एक गंभीर संदेश देता है और पाठकों को विचार करने पर मजबूर करता है कि वे कैसे अपने देश और उसके संविधान का सम्मान कर सकते हैं और असली बदलाव ला सकते हैं।
“आओ आज मनाएँ फिर लोकतंत्र का उत्सव
देशभक्त बन कर कुछ बोलें संविधान की पुस्तक खोलें
गणतंत्र का मंत्र जपें और भीड़तंत्र का हिस्सा हो लें
60. *“प्रतिफल”*
यह गीत आजादी के असली अर्थ और उसकी वर्तमान स्थिति पर एक गंभीर टिप्पणी है। कवि ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को उजागर किया है और यह दिखाया है कि कैसे आजादी के जश्न मनाए जा रहे हैं, लेकिन उनके ठोस परिणाम नहीं दिखाई दे रहे हैं।
“आजादी के जश्न बहुत हैं गुम है सब प्रतिफल
झोपड़ पट्टी में अंधियारा राजमहल रोशन
दृश्यहीन है कोहरे में संसद के अधिवेशन
अपनी-अपनी जयकारों का बढ़ता कोलाहल”
61.*“सपने बोए जाएँगे”* नवगीत आजादी के असली अर्थ और उसकी वर्तमान स्थिति पर एक गंभीर टिप्पणी है। कवि ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को उजागर किया है और यह दिखाया है कि कैसे आजादी के जश्न मनाए जा रहे हैं, लेकिन उनके ठोस परिणाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। गीत में खेती और व्यापार में हो रही गतिविधियों और व्यापारियों की प्रलोभनकारी प्रवृत्ति को दिखाया गया है। बाजार की मांग और मूल्य आधारित चयन को दर्शाया गया है।
“मंत्रमुग्ध होकर मेड़ों से लहराती फसलें देखेंगे
सौदा करती, वादा करती व्यापारी नस्लें देखेंगे
फिर लोक-समर्थन मूल्यों की उत्पादें छांटी जाएंगी।“
62. *“बसा हुआ है गाँव”*
नवगीत में कवि कहते हैं कि धारूखेड़ी गाँव अब भी उनके मन के एक कोने में बसा हुआ है। यह उनकी गहरी यादों और भावनाओं का प्रतीक है जो गाँव से जुड़ी हैं।
“मन के एक कोने में अब भी बसा हुआ है गाँव
कल-कल छल-छल हँसती गाती रूप-रेल नदी
हर सुख-दुख में साथ निभाती बीती कई सदी
तट की मनभावन हरियाली 'औं' अमराई छांव”
गीत की भाषा सरल और प्रभावी है। कवि ने गाँव की प्राकृतिक सौंदर्य, फसलों, खेल-कूद और सामाजिक गतिविधियों को सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। यह गीत सांस्कृतिक धरोहर और सामूहिकता की भावना को दर्शाता है। गाँव की चौपालों में होने वाली चर्चाएँ और रामायण की कथाएँ गाँव की सामूहिकता और सामाजिक जुड़ाव को उजागर करती हैं। कुल मिलाकर, यह गीत गाँव की सादगी, सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि को सुंदरता और संवेदनशीलता से प्रस्तुत करता है। पाठक इसे पढ़कर गाँव के जीवन की मिठास और उसकी अनमोल यादों में खो जाते हैं।
63.*“चश्मे अलग-अलग”* यह गीत व्यक्तियों के अलग-अलग दृष्टिकोण, विचारधारा, और दृष्टिकोण की विविधता को गहराई से प्रकट करता है। कवि ने चश्मे और दृष्टि के प्रतीकों का उपयोग करके यह दिखाया है कि हर व्यक्ति की सोच और दृष्टि कैसे भिन्न हो सकती है।
“सब के चश्मे अलग-अलग हैं नम्बर अलग-अलग
देख रहा है कोई सावन की हरियाली
और किसी को दिखती पूरी बगिया खाली”
यह गीत न केवल दृष्टिकोण की विविधता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे पूर्वाग्रह और स्वार्थी दृष्टिकोण व्यक्ति की दृष्टि को प्रभावित कर सकते हैं।
64.*“नाव है मझधार में”* यह गीत एक कठिन और अनिश्चित स्थिति का चित्रण करता है। कवि ने अपनी स्थिति को एक मझधार में फंसी नाव के रूप में वर्णित किया है, जहाँ पतवार जर्जर हो चुकी है और दिशाएँ अस्पष्ट हैं। विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया है, जैसे कि पतवार, मझधार, दिशा सूचक यंत्र, और आंधियाँ।
“है उपेक्षा दिशा सूचक यंत्र के व्यवहार में
आंधियों की सुन रहे हैं गूँज भी उस पार से
है खिवैया आंख मूंदे लहर से जलधार से
ध्वस्त उम्मीदें हुई हैं इसी सोच विचार में।“
यह गीत असहायता, निराशा और अनिश्चितता की भावनाओं को गहराई से प्रकट करता है। कवि ने अपने भावनात्मक और मानसिक संघर्ष को प्रभावी रूप से चित्रित किया है, जिससे पाठक उनकी स्थिति को समझ सकते हैं और उनके दर्द को महसूस कर सकते हैं।
65. *“अटूट रिश्ता है”*
इस नवगीत में कवि बताते हैं कि जब वे अकेले होते हैं, तो अक्सर उनके सामने हरसूद के दृश्य उभरते हैं। स्टेशन से घोसी मोहल्ला तक के दृश्य उनकी स्मृतियों में ताज़ा रहते हैं। यह गीत कवि की हरसूद के प्रति गहरी भावनाओं और अटूट रिश्ते को दर्शाता है। हरसूद की स्मृतियाँ कवि के मन में गहरी जड़ें जमा चुकी हैं और वे उन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे।
“यादों में हरसूद आज भी वैसा ही लगता है
मेन रोड की चहल-पहल और मधुर शोर
विद्यालय का कठिन समस्याओं को सुलझता तहसील कार्यालय का
मन फिर घायल होकर इनकी डूब व्यथा सहता है”
यह गीत सांस्कृतिक धरोहर और अटूट संबंधों की गहराई को दर्शाता है। हरसूद के विभिन्न मोहल्लों, धार्मिक स्थलों, और सामाजिक जीवन का वर्णन कवि ने अत्यंत संवेदनशीलता और प्रेम के साथ किया है। पाठक इसे पढ़कर अपने अतीत की यादों में खो जाते हैं और कवि की भावनाओं को गहराई से महसूस कर सकते हैं।
66. *“बरस कई बीते”*
नवगीत में कवि कहते हैं कि उनकी यादों का घट (घड़ा) भरा हुआ है, लेकिन खुशियों से खाली है। हरसूद को छोड़े हुए कई बरस बीत गए हैं, और इस समय के दौरान उनकी यादें तो हैं, लेकिन खुशियां नहीं रही।
“सुधियों के भरे घट खुशियों से रीते
छोड़ें हरसूद को बरस कई बीते
खूँटे पर लाकर बाँध दिया गाय-सा
दौड़ता हाँफता समय असहाय सा
गुजर गई एक उमर दिवा स्वप्न जीते”
यह गीत मनुष्य के आंतरिक संघर्ष, अतीत की यादों और वर्तमान की कठिनाइयों को चित्रित करता है। कवि ने अपनी भावनाओं और पीड़ा को गहराई से व्यक्त किया है। हरसूद को छोड़े हुए समय के साथ, कवि ने अपने जीवन की विभिन्न कठिनाइयों और संघर्षों का वर्णन किया है।
67. *“हरसूद दिखा था”*
यह गीत अतीत की यादों को संजोए हुए है। कवि ने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण स्थान हरसूद को याद करते हुए अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। हरसूद उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था, जहाँ उनकी कई सुनहरी यादें बसी हुई थीं।
“इक उम्र का हिस्सा यहीं पर रखा था कुछ सुनहरी याद की आधार शिलाएँ पास उसके लिखी हुई थी जो कथाएँ धुल गए अक्षर सभी बस 'डूब' लिखा था”
'डूब' शब्द का अर्थ हो सकता है कि उनकी सारी यादें और अनुभूतियाँ समय की धारा में बह गई हैं, जैसे कि हरसूद अब केवल एक खोई हुई याद बनकर रह गया है।
श्री रघुवीर शर्मा का गीत-नवगीत संग्रह *"नीलकंठी प्रार्थनाएं"* एक समृद्ध और विविधता से भरा काव्य संग्रह है, जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से प्रस्तुत किया गया है। श्री रघुवीर शर्मा की कविताओं में भावनाओं की गहराई और संवेदनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनकी रचनाएँ पाठकों को जीवन की जटिलताओं और मानवीय भावनाओं की गहराइयों तक ले जाती हैं।
*“नीलकंठी प्रार्थनाएं”* में प्राकृतिक सौंदर्य और दृश्यावलियों का वर्णन अद्वितीय है। कविताओं में प्रकृति के तत्वों का प्रभावशाली उपयोग किया गया है, जो पाठकों को एक अद्भुत अनुभूति प्रदान करता है। इस संग्रह में समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का विवेचन किया गया है। कविताएँ समाज की समस्याओं, संघर्षों और संस्कृतिक विविधताओं को चित्रित करती हैं। संग्रह की कविताओं में आध्यात्मिकता और प्रार्थना की भावना भी विद्यमान है, जो पाठकों को आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती हैं।
*श्री रघुवीर शर्मा* की लेखन शैली सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली है। भाषा का प्रयोग सरलता से किया गया है, जिससे कविताएँ सीधे पाठकों के हृदय तक पहुँचती हैं।
इस प्रकार, मैंने प्रत्येक रचना को अलग-अलग पढ़ा और समझा, और उनकी समग्र समीक्षा प्रस्तुत की है, जोकि न केवल रचनाकार के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, बल्कि पाठकों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती है। इस प्रयास में, मैंने किसी भी प्रकार की पूर्वाग्रह या पक्षपात से बचने का पूरा प्रयास किया है, ताकि मेरी समीक्षा वस्तुनिष्ठ और सच्ची हो सके।
आशा है कि "नीलकंठी प्रार्थनाएं" साहित्य जगत में अपार प्रतिष्ठा पाएगी और इसे पाठकों का भरपूर स्नेह मिलेगा।
सादर।
#डॉ आलोक गुप्ता
पेटेंट अटॉर्नी, आलोक गुप्ता एंड एसोसिएट्स
-“आशीर्वाद”, 626 , जवाहर कॉलोनी, नई मंडी, मुज़फ्फरनगर
मो. 9319279551
ईमेल. ashirwad626@gmail.com
14 जुलाई ,2024
 नवगीत पर एकाग्र फेसबुक पर चर्चित समूह वागर्थ समूह का संयुक्त सहयोगी उपक्रम ब्लॉग वागर्थ
नवगीत पर एकाग्र फेसबुक पर चर्चित समूह वागर्थ समूह का संयुक्त सहयोगी उपक्रम ब्लॉग वागर्थ
 नवगीत पर एकाग्र फेसबुक पर चर्चित समूह वागर्थ समूह का संयुक्त सहयोगी उपक्रम ब्लॉग वागर्थ
नवगीत पर एकाग्र फेसबुक पर चर्चित समूह वागर्थ समूह का संयुक्त सहयोगी उपक्रम ब्लॉग वागर्थ
 नवगीत पर एकाग्र फेसबुक पर चर्चित समूह वागर्थ समूह का संयुक्त सहयोगी उपक्रम ब्लॉग वागर्थ
नवगीत पर एकाग्र फेसबुक पर चर्चित समूह वागर्थ समूह का संयुक्त सहयोगी उपक्रम ब्लॉग वागर्थ
 नवगीत पर एकाग्र फेसबुक पर चर्चित समूह वागर्थ समूह का संयुक्त सहयोगी उपक्रम ब्लॉग वागर्थ
नवगीत पर एकाग्र फेसबुक पर चर्चित समूह वागर्थ समूह का संयुक्त सहयोगी उपक्रम ब्लॉग वागर्थ
 नवगीत पर एकाग्र फेसबुक पर चर्चित समूह वागर्थ समूह का संयुक्त सहयोगी उपक्रम ब्लॉग वागर्थ
नवगीत पर एकाग्र फेसबुक पर चर्चित समूह वागर्थ समूह का संयुक्त सहयोगी उपक्रम ब्लॉग वागर्थ
 नवगीत पर एकाग्र फेसबुक पर चर्चित समूह वागर्थ समूह का संयुक्त सहयोगी उपक्रम ब्लॉग वागर्थ
नवगीत पर एकाग्र फेसबुक पर चर्चित समूह वागर्थ समूह का संयुक्त सहयोगी उपक्रम ब्लॉग वागर्थ
 नवगीत पर एकाग्र फेसबुक पर चर्चित समूह वागर्थ समूह का संयुक्त सहयोगी उपक्रम ब्लॉग वागर्थ
नवगीत पर एकाग्र फेसबुक पर चर्चित समूह वागर्थ समूह का संयुक्त सहयोगी उपक्रम ब्लॉग वागर्थ
 नवगीत पर एकाग्र फेसबुक पर चर्चित समूह वागर्थ समूह का संयुक्त सहयोगी उपक्रम ब्लॉग वागर्थ
नवगीत पर एकाग्र फेसबुक पर चर्चित समूह वागर्थ समूह का संयुक्त सहयोगी उपक्रम ब्लॉग वागर्थ
 नवगीत पर एकाग्र फेसबुक पर चर्चित समूह वागर्थ समूह का संयुक्त सहयोगी उपक्रम ब्लॉग वागर्थ
नवगीत पर एकाग्र फेसबुक पर चर्चित समूह वागर्थ समूह का संयुक्त सहयोगी उपक्रम ब्लॉग वागर्थ
 नवगीत पर एकाग्र फेसबुक पर चर्चित समूह वागर्थ समूह का संयुक्त सहयोगी उपक्रम ब्लॉग वागर्थ
नवगीत पर एकाग्र फेसबुक पर चर्चित समूह वागर्थ समूह का संयुक्त सहयोगी उपक्रम ब्लॉग वागर्थ
 नवगीत पर एकाग्र फेसबुक पर चर्चित समूह वागर्थ समूह का संयुक्त सहयोगी उपक्रम ब्लॉग वागर्थ
नवगीत पर एकाग्र फेसबुक पर चर्चित समूह वागर्थ समूह का संयुक्त सहयोगी उपक्रम ब्लॉग वागर्थ
 नवगीत पर एकाग्र फेसबुक पर चर्चित समूह वागर्थ समूह का संयुक्त सहयोगी उपक्रम ब्लॉग वागर्थ
नवगीत पर एकाग्र फेसबुक पर चर्चित समूह वागर्थ समूह का संयुक्त सहयोगी उपक्रम ब्लॉग वागर्थ